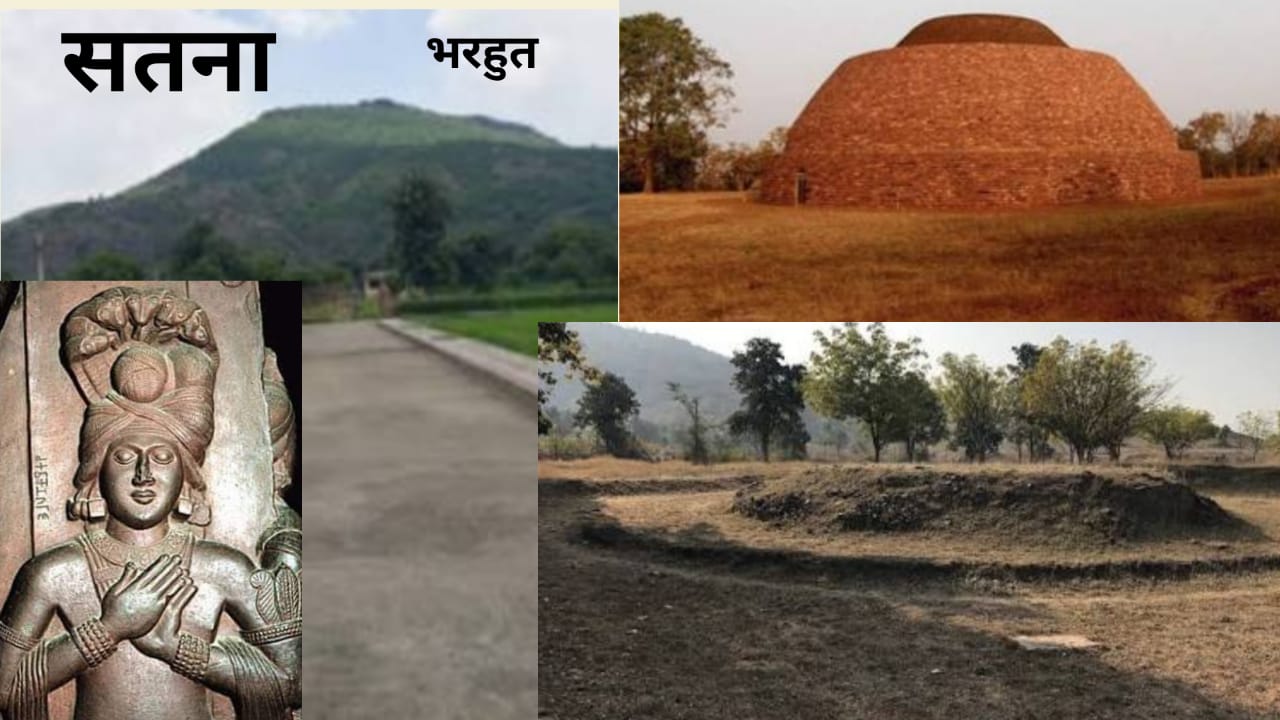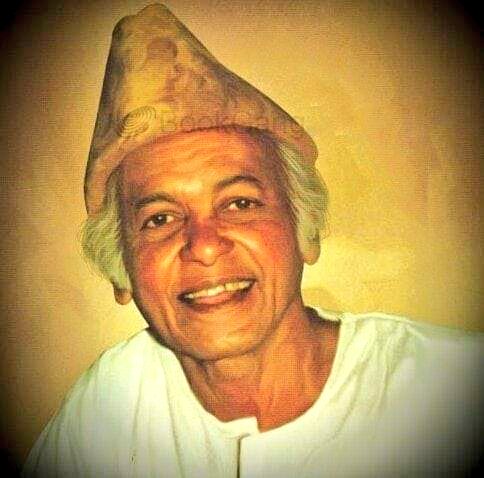◆ विश्व जैव विविधता दिवस
◆ Theme -2020: Our solutions are in Nature
◆ पृथ्वी देती है अरबों-खरबों जीवों को आश्रय
प्रतिवर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे 'विश्व जैव-विविधता संरक्षण दिवस' भी कहते हैं। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला शिल्प, संगीत, वस्त्र-भोजन, औषधीय पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव-विविधता के महत्व एवं उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। पृथ्वी के पास उसके निर्वाह और जीवंत स्वास्थ्य के लिए एक अंतर्निर्मित स्वचालन तंत्र है। धरती माता हज़ारो वर्षो से अरबों - खरबों जीवों को आश्रय देती आई है, जिनमें मानव, घरेलू जानवर, पौधे और वन्यजीव शामिल हैं। जंगली जीव-जंतु और वनस्पतियाँ इसके पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखलाओं का हिस्सा हैं। और इनकी आबादी को पृथ्वी के संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना प्रकृति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य आज पारिस्थितिक शासन को नियंत्रित करता है और विकास और लालच के लिए वैश्विक संसाधनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मनुष्य ये भूल जाता हे कि विकास और संरक्षण को संतुलन में रखना, जीविका के सिद्धांत की प्रमुख कुंजी है।
तय सीमाओं से परे पृथ्वी संसाधनों का अधिक दोहन और भारी उत्सर्जन इस ग्रह को कमजोर कर रहे हैं। उत्सर्जन के स्तर में वृद्धि से ओजोन परत के क्षरण ग्लोबल वार्मिंग, बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव, बारिश और समुद्र सूनामी आदि समस्याएं पैदा होती हैं । जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से इस ग्रह पर जीवन के अस्तित्व को खतरा है।
औद्योगिकीकरण ने परिदृश्य को और खराब कर दिया है। अनियोजित शहरीकरण, अनुपचारित शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट हमारी नदियों और अन्य जल निकायों को प्रदूषित कर रहे हैं और हमारे जलीय जीवन को भी नष्ट कर रहे हैं। साथ ही उच्च प्रदूषण का स्तर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहा है।
संक्षेप में कहें तो पृथ्वी संसाधनों के अधिक दोहन और अनियोजित विकास से उन समस्याओं की श्रृंखला शुरू हो रही है, जो अब मानव अस्तित्व को खतरे में डाल रही हैं और धरती को नुकसान पहुंचा रही हैं। यदि इस घातक प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया जाता, तो पृथ्वी इस पर्यावरण-विरोधी मानव साम्राज्य का समर्थन करने की स्थिति में नहीं रहेगी। इसलिए, हमारे अपने अस्तित्व के लिए, हमें अपनी जरूरतों से परे धरती के अपने संसाधनों का बोझ और अधिक दोहन नहीं करना सीखना होगा और हमें अपनी मिट्टी, वनस्पतियों, जीवों, हवा, नदियों, झीलों का सम्मान करना सीखना होगा और सतत विकास के सिद्धांत का सख्ती से पालन करना होगा।
पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विश्व को एकजुट होने की आवश्यकता है क्योंकि पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा है। इन सार्वभौमिक उपायों और प्रथाओं के अलावा, पृथ्वी माँ को तरो ताज़ा करने, और उसे फिर से जीवंत करने के लिए नियमित वार्षिक गतिविधि के रूप में पंद्रह से इक्कीस दिनों के अनिवार्य वैश्विक लॉकडाउन के लिए वैश्विक सहमति का समय आ गया है। यह वास्तव में मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है और हमारा कर्तव्य होगा न कि धरती माता पर उपकार।
कोविड-19 महामारी ने मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डालकर हमें सर्वोत्तम पर्यावरणीय पाठ पढ़ाया है। इस महामारी के खिलाफ दुनिया भर में लॉकडाउन ने धरती माता की कायाकल्प और पुनरावृत्ति करने की शक्ति का प्रदर्शन किया है और और मनुष्य को हमारे ग्रह की वर्तमान खराब स्थिति के लिए एक स्पष्ट अपराधी के रूप में साबित किया है।
लॉकडाउन ने उत्सर्जन स्तरों को जबरदस्त रूप से गिरा दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का स्तर लगभग चालीस प्रतिशत कम हो गया है। वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 103 भारतीय शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार हुआ है। मुंबई में प्रदूषण का स्तर सत्रह प्रतिशत कम हो गया है।
कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई जीतने के बाद, एक व्यापक अध्ययन देश में और विश्व स्तर पर व्यापक रूप से आयोजित किया जाना चाहिए जिसमे लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान के साथ - साथ इस बात का भी अध्ययन हो कि पृथ्वी और पर्यावरण कि गुणवत्ता में कितना सुधार आया हैं, प्रदूषण के स्तर में गिरावट, नदियों और अन्य जल निकायों के ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों में कमी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
उपरोक्त विश्लेषण देश के आधार पर और फिर विश्व स्तर पर, कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सबक सामने आएंगे और इन अध्ययनों के आधार पर पृथ्वी के कायाकल्प के लिए वैश्विक लॉकडाउन की योजना बनाया जा सकता है। क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व धरती माता के अस्तित्व पर निर्भर है।
डॉ मोनिका जैन
सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी