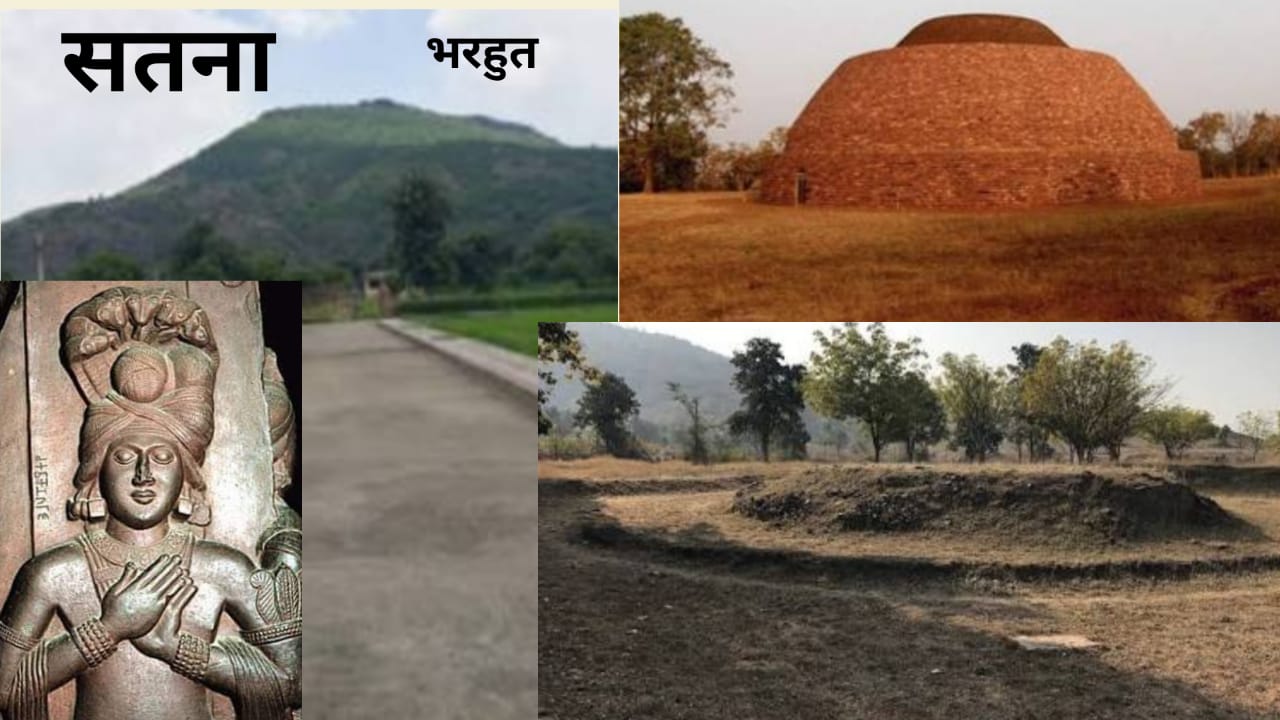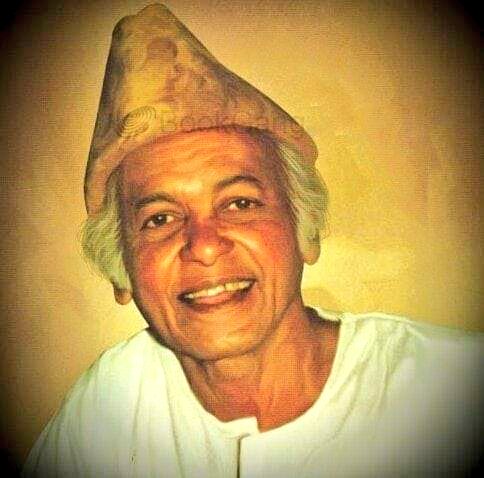◆ आरक्षण पर बीस साल पुराने गवर्नर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, कहा- जरूरतमंद SC/ST और OBC को नहीं मिल रहा उनका हक ।
◆ न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 100 फीसदी आरक्षण प्रदान करना ‘अनुचित’ होगा और कोई भी कानून यह अनुमति नहीं देता है कि अधिसूचित इलाकों में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ाएंगे। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों के 100 फीसदी पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने के जनवरी 2000 का अविभाजित आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का आदेश बुधवार को निरस्त कर दिया।
◆ न्यायालय ने कहा कि यह ‘मनमाना’ है और संविधान के अंतर्गत इसकी इजाजत नहीं है। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 100 फीसदी आरक्षण प्रदान करना ‘अनुचित’ होगा और कोई भी कानून यह अनुमति नहीं देता है कि अधिसूचित इलाकों में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ाएंगे।
युवा काफिला,नई दिल्ली -
क्या था मामला -
आंध्र प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया । जिसमें अनुसूचित जनजाति को 100 फ़ीसदी आरक्षण (जितनी भी सीट थीं सारी सीट अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित कर दी ) देने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया गया । सर्वप्रथम यह मामला जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी सरकार के निर्णय को ठीक बताया और उसको जारी रखने के लिए कहा परंतु हाईकोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को 2020 में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। जिसे 22 अप्रैल को जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें अनुसूचित जनजाति के अधिसूचित क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रप्रदेश और तेलंगाना दोनों सरकारों पर जुर्माना भी लगाया है। पीठ ने कहा कि वह वरिष्ठ वकील राजीव धवन की इस दलील से सहमत है कि आरक्षित वर्गों की सूची पर पुनर्विचार करने की जरूरत हैं ।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता । कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण नीति यह 70 साल से चली आ रहीं हैं । एक बार आरक्षण का फायदा ले चुके परिवारजनों को अब यह फायदा नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न जातियों और कबीलों के नाम एक सूची में शामिल कर दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिश्रा साहब ने पूछा कि जब आरक्षण लोगों को मिल रहा है तो भी लोग पिछड़े क्यों बने हुए हैं? आरक्षण मिलने के बाद भी कोई एक वर्ग आगे क्यों नहीं बढ़ पाया है? न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि एक बार जब हम किसी को सूची में डाल देते हैं तो उसे वही हमेशा ही क्यों रखा गया है? क्यों उसे बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया जा रहा हैं? अगर किसी व्यक्ति को अनुसूची में डाल दिया गया है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हम आदिवासी संस्कृति को बरकरार रखते हैं और फिर हम उनसे आरक्षण भी देते हैं । क्या इससे आदिवासियों की स्थिति में सुधार हुआ है या यह वैसा ही बना हुआ है ? अगर दो दशकों के आंकड़ों को देखें तो इसमें क्या सुधार हुआ है? यदि क्षेत्रों में सुधार हुआ भी है तो वह निर्भर करता है शहरीकरण पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से लॉक डाउन के दौरान नई बहस को लोगों के बीच में रख दिया है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं ? और यदि होना चाहिए तो जिन लोगों को 70 वर्षो से आरक्षण मिल रहा है उनको वापस से उनके आरक्षण की मिलने की समीक्षा होनी चाहिए या नहीं? कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान आरक्षण पर यह दूसरा लैंडमार्क जजमेंट मान सकते हैं ।
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था - सी एल प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का । 22 अप्रैल को यह जजमेंट आया है।
◆ आरक्षण नीति पर पुनः हो विचार : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट करते हुए कहा कि हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश के आदेश के खिलाफ दायर अपील में कहा गया था कि राज्यपाल का यह आदेश भेदभाव पूर्ण है क्योंकि यह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है और यह असंवैधानिक है । 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फ़ीसदी तय कर दी थी।
◆ ऐसे में 10℅ सामान्य आरक्षण क्या यह सही है ?
इंदिरा साहनी कहती हैं, "अब आरक्षण आर्धिक आधार पर दिया जा रहा ये दस प्रतिशत आरक्षण ग़लत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है इसमें भारत की अधिकतर आबादी आ जाएगी इससे जो लोग इसके बाहर रह जाएंगे ये उनके समानता के अधिकार का हनन होगा।"
वैसे आरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है । आजादी से पहले ही नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत हुई थी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए समय-समय पर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1882 - हंटर आयोग की नियुक्ति हुई। महात्मा ज्योतिराव फुले ने नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आनुपातिक आरक्षण/प्रतिनिधित्व की मांग की।
◆ कॉलेजियम सिस्टम विवादों में ?
भारत की न्यायपालिका के आंकड़े सिद्ध करते है कि भारत की न्यायिक प्रणाली में सिर्फ कुछ घरानों का ही कब्ज़ा रहा गया है। साल दर साल इन्ही घरानों से आये वकील और जजों के लड़के /लड़कियां ही जज बनते रहते हैं।जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां की जातीं हैं उसे “कॉलेजियम सिस्टम” कहा जाता है।
◆ जजों को नियुक्त करने की क्या प्रक्रिया है?
कॉलेजियम वकीलों या जजों के नाम की सिफारिस केंद्र सरकार को भेजती है। इसी तरह केंद्र भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेजती है। केंद्र के पास कॉलेजियम से आने वाले नामों की जांच/आपत्तियों की छानबीन समिति होती है और रिपोर्ट वापस कॉलेजियम को भेजी जाती है। सरकार इसमें कुछ नाम अपनी ओर से सुझाती है। कॉलेजियम; केंद्र द्वारा सुझाव गए नए नामों और कॉलेजियम के नामों पर केंद्र की आपत्तियों पर विचार करके फाइल दुबारा केंद्र के पास भेजती है। इस तरह नामों को एक - दूसरे के पास भेजने का यह क्रम जारी रहता है और देश में मुकदमों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है।
यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि जब कॉलेजियम किसी वकील या जज का नाम केंद्र सरकार के पास “दुबारा” भेजती है तो केंद्र को उस नाम को स्वीकार करना ही पड़ता है, लेकिन “कब तक” स्वीकार करना है इसकी कोई समय सीमा नही है।
UPA सरकार ने 15 अगस्त 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगह NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) का गठन किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक करार दे दिया । ताकि भारत की न्यायपालिका पर कुछ निश्चित घरानों का ही कब्ज़ा बना रहे । इस प्रकार जजों की नियुक्ति और तबादलों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम ही करता है।
ऊपर दी गयी पूरी जानकारी के आधार पर यह बात स्पष्ट हो गया है कि देश की मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था “हलवाई का लड़का हलवाई” बनाने की तर्ज पर “जज का लड़का जज” बनाने की जिद करके बैठी है। भले ही इन जजों से ज्यादा काबिल जज न्यायालयों में मौजूद हों। यह प्रथा भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश के लिए स्वास्थ्यकर नही है। कॉलेजियम सिस्टम का कोई संवैधानिक दर्जा नही है।इसलिए सरकार को इसको पलटने के लिए कोई कानून लाना चाहिए ताकि भारत की न्याय व्यवस्था में काबिज कुछ घरानों का एकाधिकार ख़त्म हो जाये।