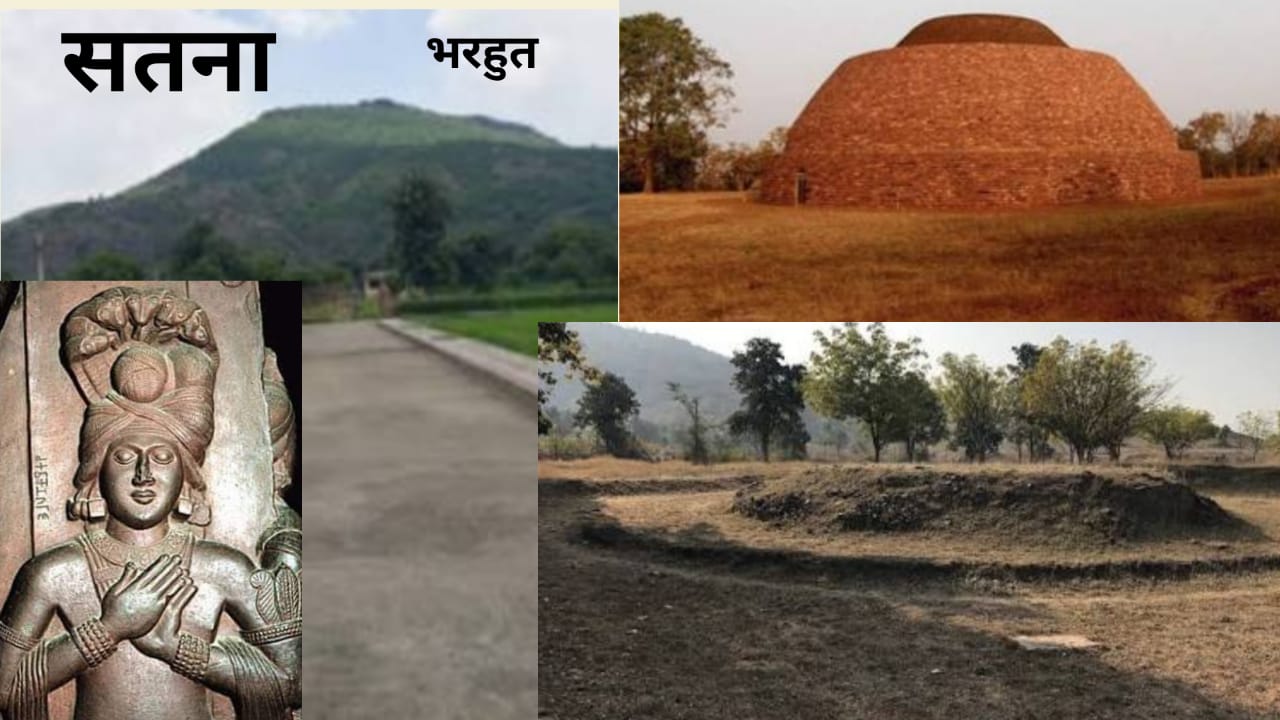(कांशीराम जयंती विशेष) -
मास्टर चाबी-
किसी भी ताले को खोलने के लिए चाहिए चाबी। पंजाबी भाषा में कहें तो किल्ली और हर किस्म का ताला खोले जो चाबी वो कहाए गुरकिल्ली (मास्टर की) दलितों को ये मास्टर चाबी थमाई कांशीराम ने । आजादी के बाद कांग्रेस ब्राह्रमणों, दलितों और मुसलमानों के वोट पाकर सत्ता में पहुंचती थी। सत्ता के शीर्ष पर कोई ब्राह्मण या ठाकुर ही बैठता था। कुछ दलितों को कैबिनेट में एडजस्ट कर लिया जाता था। इसी एडजस्टमेंट की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जो सबसे ऊपर पहुंचे। वह थे बाबू जगजीवन राम। बाबू जी बिहार के दलित नेता थे। इनकी बेटी मीरा कुमार सासाराम से सांसद रही हैं और बाद में स्पीकर भी।
एक सरकारी मुलाजिम नौकरी छोड़ कभी साइकिल तो कभी रेलवे की सेकंड क्लास से सफर कर एक मूवमेंट खड़ा कर रहा था। वह लोगों के घर-घर जाता और उनसे बात करता उसका नाम था मान्यवर कांशीराम वह जानता था कि आंबेडकर के ज्ञान की बदौलत ही आज दलित उच्च शिक्षा ग्रहण तो कर रहा हैं लेकिन आंबेडकर ने किताबे जन-जन तक पहुँचायी और मैंने लोगों को इकट्ठा किया। उस व्यक्ति का नाम मान्यवर कांशीराम था।
कितनी तारीख है आज? 15 मार्च यही तारीख तब भी थी। साल था 1934 , पंजाब के रोपड़ जिले के पिरथीपुर बंगा गांव में उनका जन्म हुआ। अब बहुजन आंदोलन से जुड़े लोग इस गांव में बने मान्यवर कांशीराम के घर को चन साहिब पुकारते हैं। चन का अर्थ होता है घर । साहिब कांशीराम के लिए उपाधि के तौर पर इस्तेमाल होता है।
मान्यवर कांशीराम को 1957 में पहली सरकारी नौकरी मिली सर्वे ऑफ इंडिया में , मगर उन्होंने बॉन्ड साइन करने से इनकार कर दिया। फिर अगले ही साल 1958 में एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डिवेलपमेंट लैबोरेटरी में बतौर रिसर्च असिस्टेंट नौकरी मिल गई। तैनाती हुई पूना (अब पुणे) में ) । पूना अपने आप में विशिष्ट पहचान रखता हैं यहीं से ज्योतिबा फुले का शिक्षा का कारवां अपनी जीवनसंगिनी सावित्री और उनकी साथी फातिमा शेख के साथ शुरू हुआ था और यहीं से उनके जीवन की शुरुआत हुई।
महाराष्ट्र संतों की भूमि-
महाराष्ट्र की भूमि संतों और महापुरुषों की कर्म स्थली रहीं हैं और दलित आंदोलन की जड़े डॉ आंबेडकर के कारण महाराष्ट्र में गहरी थी। साहित्य में, संगीत में, समाज में प्रतिरोध के स्वर गहरे थे लेकिन कई अंतरविरोध भी थे और कांशीराम के वक्त जो आंदोलन हुए उनमें समाज कई धड़ों में बंटा हुआ था। इन हालातों के बीच उनके DRDO ऑफिस में जयंती कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद जिसने उन्हें एक खत लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके पहले उन्होंने रात भर में कई बार (Annihilation of Cast) जात पात का विनाश नामक ग्रंथ जो डॉ आंबेडकर द्वारा जातपात तोड़क मंडल के लिए लिखा था परंतु किसी कारणवश वह कार्यक्रम टाल दिया गया और वो भाषण छप नहीं पाया था ।
उन्होंने अपने घरवालों को पूरे 24 पन्ने का एक पत्र भेज दिया।इसमें उन्होंने लिखा कि-
1. आज के बाद मैं कभी घर नहीं आऊंगा।
2. कभी कोई अपना घर/प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा।
3. गरीबों-दलितों का घर ही मेरा घर होगा।
4. सभी रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा।
5. किसी के शादी, जन्मदिन, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होऊंगा।
6. कोई नौकरी नहीं करूंगा।
7. जब तक डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर का सपना पूरा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठूंगा।
कांशीराम ने इन प्रतिज्ञाओं का पालन सम्पूर्ण जीवन किया। वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए।वह जिस जमात की लड़ाई लड़ रहे थे। वह कई चीजों से जूझ रही थी. जाति, अशिक्षा, गरीबी। कांशीराम ने तय किया कि तय राजनैतिक गुलामी को तोड़ना होगा। कलफ का कुर्ता पहनकर गांधीवादी बातें करके अपनी बिरादरी का भला होने से रहा।वह सेकंड हैंड कपड़ों के बाजार से अपने लिए पैंट कमीज खरीदने लगे। कभी नेताओं वाली यूनिफॉर्म नहीं पहनी। बाद के दिनों में सफारी सूट पहनने लगे।
5 रुपये का सूट-
एक समय की बात हैं कांशीराम के पास 5 रुपये थे और वे दिल्ली के कैनोट प्लेस में सूट खरीदने गए सूट पसंद भी आ गया परंतु वह था 200 रुपये का तब दुकानदार द्वारा उन्हें दुतकार दिया गया परंतु उन्होंने हर नहीं मानी और उसी से पूछ बैठे - ये 5 रुपये का सूट कहा मिलेगा? दुकानदार ने भी बड़े गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा वहां श्मशान हैं वहीं मिलेगा तुम्हें 5 रुपये का कोट । तब उन्होंने तुरंत श्मशान की ओर दौड़ लगा दी और ले आये 5 रुपये का कोट ।
राजनीतिक कैरियर-
सर्वप्रथम 1964 में उन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन की । कुछ ही बरसों में कांशीराम को समझ आ गया कि आरपीआई चुनावों में हिस्सा तो लेती है। मगर सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों में जो दलित पिछड़े शोषित तबके के लोग हैं, उन्हें साथ लाने का कोई प्रोग्राम इनके पास नहीं हैं और सत्ता में बने रहने का और उसे औजार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भी जिस डिजाइन की जरूरत है, वह इनके पास नहीं हैं।
फिर कांशीराम ने पूरा देश सायकिल से नाप लिया। अलग अलग तबके और राज्यों के लोगों से मिले और उनकी परेशानियों को समझा। डॉ आंबेडकर के जन्मदिन के दिन 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉईज फेडरेशन (बामसेफ) का गठन किया। 6 दिसंबर 1978 को इस संगठन को नए सिरे से दुरुस्त किया । इसके बाद 1981में बना डीएस -4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति । इनके कामकाज के सिलसिले में कांशीराम ने फिर देश घूमा तो उन्हें सबसे ज्यादा गुंजाइश उत्तर प्रदेश में समझ आई। पंजाब में भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। 1984 में बीएसपी के गठन के साथ ही कांशीराम चुनावी राजनीति में कूद पड़े। उन दिनों कही कांशीराम की एक बात योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के दिनों में बहुत दोहराते थे।
पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए और फिर तीसरे चुनाव से जीत मिलनी शुरू हो जाती है।
पहले चुनाव में इंदिरा लहर के दौरान बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। मगर हिम्मत खुल गई और दलितों की अपनी पार्टी अस्तित्व में आई। मनुवाद और ब्राह्मणवाद को खुले आम गरियाती, गांधी को और कांग्रेस को सिरे से खारिज करती, इस दौरान सधे हुए शब्द नहीं तलाशे जाते। खुंखार और खुरदुरे ढंग से कहा जाता। इसी दौर में नारे आए थे- ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर, बाकी सब हैं डीएस 4।
या फिर - तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हालांकि बीएसपी अब आधिकारिक तौर पर इन नारों को अपने से नहीं जोड़ती। कांशीराम की शिष्या मायावती समझ गई हैं कि कोर वोट के आगे बढ़ने के लिए बहुजन को सर्वजन में बदलना होगा।
कांशीराम 1984 के चुनाव के बाद ये तय कर चुके थे कि रसरी को तब तक आना जाना होगा, जब तक सिल पर निसान न बने। इसलिए उन्होंने राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान पश्चिम यूपी में जब भी उपचुनाव हुए, मायावती को मैदान में उतारा। एक बार बिजनौर से, एक बार हरिद्वार से और आखिर में 1989 के चुनाव में इसी बिजनौर सीट से बीएसपी का खाता खुला। मायावती लोकसभा पहुंचीं। इस चुनाव में कांशीराम ने देश के अगले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ इलाहाबाद से चुनाव लड़ा।
बीएसपी का मूवमेंट लगातार मजबूत होता गया। राममंदिर और मंडल के दौर में कांशीराम ने अपने मूल सपने की तरफ लौटना रणनीतिक तौर पर मुनासिब समझा। उनकी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की नई नई बनी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद 1993 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। बीएसपी के मिशनरी कार्यकर्ता अब माननीय कैबिनेट मंत्री थे।
कांशीराम समझ गए थे कि मायावती ही उनकी राजनीतिक वारिस होंगी। तेर- तर्रार भाषण शैली, संगठन क्षमता और कड़ाई के साथ काडर से अपनी बातें मनवाना। जल्द ही मायावती की यह स्टाइल मुलायम सिंह को अखरने लगी। उधर मौके की तलाश में बैठे बीजेपी के पॉलिटिकल मैनेजरों ने कांशीराम को अपनी बात समझाई। कांशीराम तो कब से यही चाहते थे। सवर्णों की पार्टी के कंधे पर चढ़ दलित की बेटी पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बन गई ।कांशीराम के मिशन की ये पहली बड़ी कामयाबी थी।
एक समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साहब कांशीराम को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया , लेकिन कांशीराम ने यह प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया। उन्होंने कहा - मैं राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ।
फिर उन्होंने नारा दिया -
‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’। वे रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनकर चुपचाप अलग - थलग बैठने के लिए तैयार नहीं थे।
लेकिन आज तक इस बात पर चर्चा नहीं होती कि आख़िर अटल बिहारी वाजपेयी कांशीराम को राष्ट्रपति क्यों बनाना चाहते थे???
कहते हैं कि राजनीति में प्रतिद्वंद्वी को प्रसन्न करना उसे कमज़ोर करने का एक प्रयास होता हैं। ज़ाहिर है आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए वाजपेयी इसमें कुशल थे। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो वे कांशीराम को पूरी तरह समझने में चूक गए। वरना वे निश्चित ही उन्हें ऐसा प्रस्ताव नहीं देते। वाजपेयी के प्रस्ताव पर कांशीराम की इसी अस्वीकृति में उनके जीवन का लक्ष्य भी देखा जा सकता है। यह लक्ष्य था सदियों से ग़ुलाम वंचित वर्ग को सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदे पर बिठाना।
मायावती के रूप में उन्होंने एक लिहाज से ऐसा कर भी दिखाया। कांशीराम पर आरोप लगे कि इसके लिए उन्होंने किसी से गठबंधन से वफ़ादारी नहीं निभाई। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी से समझौता किया और फिर ख़ुद ही तोड़ भी दिया। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि कांशीराम ने इन सबसे केवल समझौता किया, गठबंधन उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए किया। इसके लिए कांशीराम के आलोचक उनकी आलोचना भी करते रहे हैं। लेकिन कांशीराम ने इन आरोपों का जवाब बहुत पहले एक इंटरव्यू में दे दिया था। उन्होंने कहा था, ‘मैं उन्हें (राजनीतिक दलों) ख़ुश करने के लिए ये सब (राजनीतिक संघर्ष) नहीं कर रहा हूं।'
अपने राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के दौरान कांशीराम ने, उनके मुताबिक़ ब्राह्मणवाद से प्रभावित या उससे जुड़ी हर चीज़ का बेहद कटु शब्दों में विरोध किया, फिर चाहे वे महात्मा गांधी हों, राजनीतिक दल, मीडिया या फिर ख़ुद दलित समाज के वे लोग जिन्हें कांशीराम ‘चमचा’ कहते थे। उनके मुताबिक ये ‘चमचे’ वे दलित नेता थे जो दलितों के ‘स्वतंत्रता संघर्ष’ में दलित संगठनों का साथ देने के बजाय पहले कांग्रेस और बाद में भाजपा जैसे बड़े राजनीतिक दलों में मौक़े तलाशते रहे हैं।अपनी चर्चित किताब ‘चमचा युग’ में कांशीराम ने इसके लिए महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि आंबेडकर की दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को गांधीजी ने दबाव की राजनीति से पूरा नहीं होने नहीं दिया और पूना पैक्ट के फलस्वरूप आगे चलकर संयुक्त निर्वाचक मंडलों में उनके ‘चमचे’ खड़े हो गए।
कांशीराम ने लिखा है, ‘औज़ार, दलाल, पिट्ठू अथवा चमचा बनाया जाता है सच्चे, खरे योद्धा का विरोध करने के लिए। जब खरे और सच्चे योद्धा होते हैं चमचों की मांग तभी होती है। जब कोई लड़ाई, कोई संघर्ष और किसी योद्धा की तरफ से कोई ख़तरा नहीं होता तो चमचों की ज़रूरत नहीं होती, उनकी मांग नहीं होती। प्रारंभ में उनकी उपेक्षा की गई। किंतु बाद में जब दलित वर्गों का सच्चा नेतृत्व सशक्त और प्रबल हो गया तो उनकी उपेक्षा नहीं की सजा सकी। इस मुक़ाम पर आकर, ऊंची जाति के हिंदुओं को यह ज़रूरत महसूस हुई कि वे दलित वर्गों के सच्चे नेताओं के ख़िलाफ़ चमचे खड़े करें।’
1996 में कांग्रेस के साथ बीएसपी का गठबंधन हुआ और मायावती का दो बार और बीजेपी संग गठबंधन कर मुख्यमंत्री बनना। 2007 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना। इन सबके पीछे कांशीराम की दिन रात की मेहनत, रणनीति और बुलंद इरादों की पृष्ठभूमि है। हालांकि उन पर ये इल्जाम भी लगा कि आखिर में उन्होंने संगठन पूरी तरह से मायावती को सौंप दिया। कठिन दिनों के तमाम साथियों की तरफ से आंखें मूंद लीं। कांशीराम का यही कहना है कि मुझे मायावती में ही नेतृत्व की सर्वश्रेष्ठ संभावना दिखी। इसलिए मैंने उन्हें नेतृत्व सौंपा।